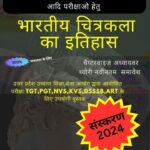आज हम जानेगे संयोजन के सिद्धान्त के बारे मे जो चित्रकला के कार्य के लिए बहुत ही आवश्यक है पिछली पोस्ट मे हमने कला के तत्वो का जाना था इसको पढ़ने के लिए हमारी पोस्ट कला के तत्व पर जाये
संयोजन के सिद्धांत कितने हैं?
संयोजन के सिद्धान्त
संयोजन के 6 सिद्धान्त होते है
1 सहयोग
2 सामजस्य
3 संतुलन
4 प्रभाविता
5 प्रवाह /लय
6 प्रमाण /अनुपात
note – tgt-pgt nvs kvs net -jrf आर्ट की परीक्षा के लिए आप जो ये हमारी पोस्ट पढ़ रहे अगर आपको हमारी ebook खरीदनी है जो की भारतीय चित्रकला का इतिहास 478 page की ebook है इसे आप आसानी से amazon.in पर खरीद सकते है इसका लिंक नीचे दिया गया है
Buy link –https://www.amazon.in/dp/B0DC4X4RPG
चित्रकला में संयोजन का अर्थ क्या है?
संयोजन दो या दो से अधिक तत्वो की मधुर योजना को संयोजन कहते है ।
जब कलाकार चित्र के तत्व रेखा रूप रंग तान आदि को सुनियोजित रूप व कलात्मक रूप मे प्रयोग करके अपनी भावनाओ की अभिव्यक्ति चित्र के रूप मे करता है तो वह संयोजन कहलाता है ।
संयोजन को प्रभावी बनाने के लिए चित्रकला के तत्वो का प्रयोग संयोजन के सिद्धान्त के आधार पर किया जाता है ।
1. सहयोग /एकता
सहयोग का अर्थ है की चित्र संयोजन के विभिन्न तत्वो मे अनुभूत एकता ,समानता तथा एक प्रकार का सम्बंध जो समस्त संयोजन को एकता के सूत्र मे पिरोये रहता है । चित्र के विभिन्न तत्वो के इस तर्क -संगत संबंध को सहयोग कहते है।
प्रत्येक चित्र का अपना एका लक्ष्य होता है ।ओर जब उसके सभी तत्व एक दूसरे से संबन्धित होकर एक ही लक्ष्य लक्षित करते हो तभी चित्र मे सहयोग भाव उत्पन्न होता है कला रचना सहयोग की स्थिति के स्तर से प्रारम्भ होती है अर्थात जो दिखाई दे रहा है उसमे बिखराव नहीं होना चाहिए यही सहयोग का कार्य है ।इस तरह से हम कह सकते है की सहयोग का तात्पर्य है चित्र के सभी तत्वो रेखा , रूप वर्ण ,तान पोत सभी मे सहयोग स्थापित है ।
2. सामजस्य –
सामजस्य कला सृजन का वह सिद्धान्त है जिसके अनुसार चित्रण के सदभी तत्व यथा वर्ण ,तान एवं रूप आदि एक दूसरे के साथ मेल खाते हुए प्रतीत हो तथा चित्र मे निरर्थक विकर्षण -तत्व न आने पाये । जब किसी समूह के सभी अंग शक्तिशाली सादृश्य से बंधे हो तो वह सामजस्य चयन का उदाहरण कहा जा सकता है ओर जब इन अंगों को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाये की वे सब समस्त कलाकृति के अनुरूप ढल जाये तो सामजस्य चयन के साथ -साथ सामजस्य व्यवस्था भी होती है । चित्र मे सादृश्य भाव किस सीमा तक रहे , ही चित्र विशेष का विषय है परंतु विरोधाभास यदि मात्र आकर्षण के लिए है तो यह उचित है अन्यथा वह सामजस्य के लिए घातक भी हो सकता है । अतः अनुभव यह बताता है की चित्र मे समाविष्ट बड़ी वस्तुओ मे किसी प्रकार का सादृश्य रहना चाहिए जबकि छोटी वस्तुओ मे परिवर्तन के लिए विरोधाभास का पुट दिया जा सकता है ।
कलाकृति मे सबसे सुंदर सामजस्य वर्णो का सामजस्य होता है ।
सर्वाधिक सामजस्य उत्पन्न करने वाले वर्ण पीला व उसके सजातीय वर्ण होते है ।
3. संतुलन (balance )
संतुलन एक ऐसा सिद्धान्त है , जिसके माध्यम से चित्र के विरोधी तत्वो को व्यवस्थित किया जाता है । संतुलन के अंतर्गत चित्र मे रेखा , रूप रंग सभी को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है की कोई भी तत्व अनावश्यक भारयुक्त प्रतीत न हो , यदि ऐसा हुआ तो चित्र असंतुलित हो जाएगा , उदाहरण – यदि कलाकार चित्र के एक भाग मे कुछ रूपाकृति अंकित करता है ओर संतुलन का दूसरा भाग रिक्त छोड़ देता है , तो यह गलत होगा क्योंकि इससे अंतराल के उस भाग का भार बहुत बढ़ जाएगा जिससे रूपो की रचना हुई है ओर इसके विपरीत अंतराल का रिक्त भाग भार शून्य लगेगा । अतः इसे सही अंतराल के रिक्त भाग मे भी कुछ रूपो का निर्माण करना चाहिए तभी चित्र संतुलित होगा ।
संतुलन मानव जीवन का आधार है । यह जीवन की गतिशीलता को आधार प्रदान करता है ।
संतुलन कला सर्जन का वह सिद्धान्त है जिसके अनुसार चित्र के तत्व रेखा ,रंग ,रूप सभी तत्वो को इस प्रकार स्थापित करना ही पूरे चित्रतल पर बराबर बांटा जाये ।
संतुलन का सर्वश्रेष्ट उदाहरण ताजमहल है ।
4. प्रभाविता
चित्र मे प्रभाविता का तात्पर्य उस सिद्धान्त से है तथा उसके बनाए हुए चित्र पर सर्वाधिक प्रभाव डालता हो दृष्टि पड़ती हो तथा उसके बाद महत्व के अनुसार चित्र के अन्य तत्व पर नजर पड़ती हो ।
प्रभाविता के तीन प्रमुख उद्देश्य है
1 एकरसता को समाप्त करना
2 चित्रित वस्तु आकृति के रूप को सरलता प्रदान करना , क्योंकि हमारी दृष्टि हमेशा महत्वपूर्ण आकृतियो ओर आकर्षित होती है ।
3 मुख्य विचार की अभिव्यक्ति करने वाले तत्वो को प्रभाविता प्रदान कर चित्र मे सहयोग के प्रभाव को उत्पन्न करता है ।
प्रभाविता के तत्व –
प्रभाविता के लिए तत्व मुख्य रूप से उत्तरदाई है –
1 विषयवस्तु की अनुरूपता
2 साधारणीकरण
साधारणीकरण ओर विषयवस्तु की अनुरूपता के उदाहरण भारतीय लघु चित्रो मे पाये जा सकते है ।
5. प्रवाह
प्रवाह का अर्थ चित्रतल पर नजर का स्वतंत्र व आबाद एवं मधुर विचरण गति होती है ।
प्रवाह पूर्ण चित्र मे कभी भी गति को उलझन की स्थिति को या कष्टदाय स्थिति का सामना नहीं करना पड़ता है ।
यह गति रेखा , रंग ,रूप तथा तान सभी मिलकर उत्पन्न करते है ।
रिक्त स्थान मे गति नहीं होती है परंतु जैसे ही हम उसमे कोई आकार बनाते है हमारी दृष्टि वही ठहर जाती अन्य आकार भी बना देने से दृष्टि को गति प्राप्त होती है ।
सरल गति –
एक स्थान से दूसरे स्थान तक खींची गई रेखा ।
कोणीय गति –
ये टूटी फूटी रेखा के समान होती है , जटिल कोण अचानक दृष्टि के मार्ग को अवरूद्ध कर उसे अन्य दिशा मे मोड देते है । रचन मे इसका अधिक प्रयोग दृष्टि को थका देता है ।
लहरदार –
सर्पकार के अनुरूप होती है गति का यह प्रकार जटिल एवं रोचक होता है ।
कला के तत्व ,कला के कितने भाग होते हैं? चित्रकला का कौन-सा तत्व सबसे महत्वपूर्ण है और क्यों?
कला का अर्थ , कला के प्रकार ,कला की परिभाषा
रंगो का महत्व ,रंग कितने प्रकार के होते है ?,रंग योजना,रंगो की विशेषता एव प्रभाव
6 . प्रमाण
लंबाई चौड़ाई का आपसी संबंध तथा सभी आकृतियो का एक दूसरे से संबंध ओर चित्र के सभी तत्वो का आपस मे संबंध । पारस्परिक संबंध होने के कारण प्रमाण को संबंधता का सिद्धान्त भी कहते है ।
प्रमाण का सर्वप्रथम कारी होता है चित्र को रूचिकर बनाना व चित्र मे नीरसता आने से बचाना है ।
इसमे विभाजन व्यवस्था ऐसे की जाती है की बड़ी इकाई , छोटी इकाई से उसी अनुपात मे संबन्धित होती है जो संबंध बड़ी इकाइ से होता है । प्राचीन मिस्त्र्व यूनानी कलाकारो ने इस सिद्धान्त का प्रयोग कला की प्रत्येक रचना मे किया है।
मानव शरीर प्रमाण का सर्वश्रेष्ट उदाहरण है ।
माइकल एंजिलों के अनुसार मानवाकृति को आठ भागो मे विभाजित करके प्रमाण निश्चित किया जाता है ।
प्रमाण प्रयोग के व्यवस्थित उदधारण सर्वप्रथम मिस्त्र से प्राप्त होते है पिरामिड
ओर पढे
हमारा youtube channel studyglob fact2@ को जल्दी subscribe कीजिये ओर नोटिफ़िकेशन को ऑन कीजिये ताकि सारी विडियो की जानकारी आपको मिलती रहे धन्यवाद
youtube लिंक –https://www.youtube.com/@studyglobfact2
चित्रकला षडांग ,भारतीय चित्रकला के 6 अंग
परिप्रेक्ष्य –
परिप्रेक्ष्य एक वैज्ञानिक सिद्धान्त है । इस सिद्धान्त के द्वारा द्वियायमी चित्र भूमि पर रूपाकृति को त्रिआयामी प्रभाव दिखाते हुए ठोस व प्रमाण युक्त बनाया जाता है ।
परिप्रेक्ष्य दो प्रकार का होता है
1 वायवीय –
इसमे नजदीक की वस्तु साफ दिखाई देती है व दूर की वस्तु धुँधली दिखाई देती है ।
2 रेखीय –
इसमे दूर जाती हुई वस्तु एक बिन्दु पर मिलती हुई दिखाई देती है जैसे रेल की पटरिया ।
सामान्यत हमारी दृष्टि प्रत्येक वस्तु को अंतराल मे उसकी लंबाई ,चौड़ाई तथा गहराई इन तीनों आयामो मे ग्रहण करती है पर चित्रतल हमेशा द्वि आयामी होते है लंबाई ,चौड़ाई
तीसरे आयाम 3D का भ्रम उत्पन्न करने के लिए जिस तरीके विधि या प्रविधि का प्रयोग किया जाता है उसे परिप्रेक्ष्य प्रणाली कहते है
यह भ्रम भी कहलाता है । जैसे आसमान एक निश्चित दूरी पर पृथ्वी से मिलता हुआ प्रतीत होता है , रेल पटरी दूर होती हुई आगे जाकर मिलती हुई दिखाई देती है ।
note – tgt-pgt nvs kvs net -jrf आर्ट की परीक्षा के लिए आप जो ये हमारी पोस्ट पढ़ रहे अगर आपको हमारी ebook खरीदनी है जो की भारतीय चित्रकला का इतिहास 478 page की ebook है इसे आप आसानी से amazon.in पर खरीद सकते है इसका लिंक नीचे दिया गया है
Buy link –https://www.amazon.in/dp/B0DC4X4RPG
इन्हे भी पढ़े –
- छापा कला क्या है ?,छापाकला का विकास कब से प्रारम्भ हुआ,छापा कला कितने प्रकार की है ,मूर्तिकला (मूर्ति बनाने के विधिया
- भारत मे स्थित स्थलो के खोजकर्ता एव समय
- भारत मे स्थित प्रमुख राष्ट्रीय संग्रहालय टीजीटी , पीजीटी आर्ट , यूपीएससी ओर अन्य exam के लिए महत्वपूर्ण जानकारी 2023 update
- चित्रकला के तत्व
- भारत के महत्वपूर्ण कला ग्रुप
- भारत की कला संबन्धित पुस्तक व लेखक ,भारतीय चित्रकार ,भारतीय मूर्तिकार ,प्रिंटमेकर कलाकार
- भारत के प्रमुख वाद , विश्व के प्रमुख वाद ,प्रमुख यूरेपियन शैलिया का उदय, भारत के घनवादी कलाकार
- भारतीय चित्रकारों द्वारा बनाए गए चित्र श्रंखला, भारतीय चित्रकारों के नाम व उनको दी गई उपाधि व उपनाम , भारत के प्रमुख नगर एव उनके वास्तुकार
- भारत के प्रमुख कार्टूनिस्ट,अशोक के शिलालेख,भारत के महत्वपूर्ण मन्दिर ,भारत के प्रमुख दर्शनीय स्थल
- भारत मे स्थित स्थलो के खोजकर्ता एव समय
- कला के क्षेत्र मे भारत रत्न, पदम विभूषण ,पदम भूषण ,पदम श्री ,कालिदास सम्मान ,से सम्मानित कलाकार
- महत्वपूर्ण ग्रंथ व लेखक के नाम
- पहाड़ी चित्रकला शैली (1700-1900)ई0 उप शैलिया, उत्कर्ष काल ,एव सम्पूर्ण पहाड़ी शैली कि विशेषताए
- मण्डी शैली
- कुल्लू शैली
- कांगड़ा शैली
- चम्बा शैली के चित्रकार ,विषय वस्तु , एव विशेषताए
- बसोहली शैली का चरमोत्कर्ष काल ,चित्रो कि खोज, प्रमुख चित्रकार ,विषय वस्तु एव विशेषताए
- गुलेर शैली कि स्थापना ओर प्रमुख चित्रकार , एव विशेषताए 2023 update
- सिंधु घाटी की सभ्यता (the indus valley civilization )3500 ईसा पू0 से 2500 ईसा पू0 टीजीटी, पीजीटी art ,upsc exam के लिए 2023 अपडेट
- https://studyglob.com/
- अजंता की गुफाये (200 ईसा पूर्व से 650 ईस्वी तक ) टीजीटी,पीजीटी ,upsc,net ,jrf तैयारी के लिए 2023 अपडेट
- एलोरा गुफा ( राष्ट्रकूट काल 4 वीं शती -12 वीं शती ) tgt ,पीजीटी, upsc व अन्य इतिहास की जानकारी के लिए 2023अपडेट
- जोगीमारा की गुफा मौर्यकालीन गुफा 300 ईसापूर्व tgt,pgt,upsc व अन्य सरकारी नौकरी के लिए 2023 update
- सिततनवासल की गुफा (पांडव काल ) 7 वीं शताब्दी से 9 वीं शती ( टीजीटी ,पीजीटी ,यूपीएससी net ,jrf की महत्वपूर्ण जानकारी के लिए 2023 अपडेट )
- बाघ गुफा (बौद्ध कालीन 200 ईसा पूर्व से 600 ईशवी ) 2023 अपडेट
- एलिफैण्टा की गुफा ( 600 ई. से 900 ई . ) का रोचक इतिहास 2023 update tgt pgt art ke liye जरूर पढ़ें
- बादामी गुफा ( चालुक्य काल ) 650-1000 ई. tgt,pgt, upsc exam के लिए महत्वपूर्ण जानकारी 2023 अपडेट
- भीमबेटिका गुफा टीजीटी,पीजीटी,art ,upsc ,नेट,jrf exam के लिए महत्वपूर्ण 2023 update
- कला के तकनीक माध्यम
- कला के तत्व ,कला के कितने भाग होते हैं? चित्रकला का कौन-सा तत्व सबसे महत्वपूर्ण है और क्यों?
- चित्रकला षडांग ,भारतीय चित्रकला के 6 अंग
- कला का अर्थ , कला के प्रकार ,कला की परिभाषा
- संयोजन के सिद्धान्त व परिप्रेक्ष्य
- भारतीय चित्रकला का इतिहास
- राजस्थानी शैली
- मेवाड़ शैली
- मारवाड़ शैली
- हाड़ौती शैली
- ढूँढार शैली
- मुगल काल ,जंहागीर काल शाहजंहा ,औरगजेब
- मुगलकालीन चित्रकला
- नाथद्वार शैली
- बंगाल शैली अवनीन्द्रनाथ टैगोर
- गुजराती शैली, अपभृंश शैली
- कम्पनी शैली
- राजा रवि वर्मा
- बंगाल शैली अवनीन्द्रनाथ टैगोर
- गगेन्द्रनाथ टैगोर
- ई0वी0 हैवल
- असित कुमार हल्दार
- नंदलाल बसु
- देवी प्रसाद राय चौधरी
- शैलेंद्र नाथ डे
- यामिनी राय
- क्षितिंद्रनाथ मजूमदार
- के.वेंकटप्पा
- मुकुल चन्द्र डे
- रबीन्द्रनाथ टैगोर Rabindranaath taigore
- अब्दुर रहमान चुगताई Abdur Rahman Chugtai
- अमृता शेरगिल Amrita Shergil
- हेलेनिस्टिक युग (Hellenistic Period )
- शास्त्रीय युग (classical Period )
- क्रीटन माइसीनियन तथा यूनानी कला
- मेसोपोटामिया की कला
- मिस्त्र की कला
- सल्तनत कला
- वैदिक कला
- भूपेन खक्खर
- सोमनाथ होर Somnath Hor
- रामगोपाल विजयवर्गीय